एहतराम - अज़ीम शायरों को सलाम ( अंक - ०२ )
आवाज़ मशहूर ग़ज़ल गायक शिशिर पारखी के साथ मिल कर संगीतमय स्मरण कर रहा है उस्ताद शायरों का, जिन्होंने ग़ज़ल लेखन को बुलंदियां से नवाजा. हम थे ग़ज़ल के सुनहरे दौर में जहाँ एक शाहंशाह जो ख़ुद भी शायर था और जिसके दरबार में हर शाम ग़ज़लों की महफिलें आबाद होती थी. मोमिन खान मोमिन के बाद आईये ज़िक्र करें इब्राहीम ज़ौक का. पहले सुन लेते हैं इस दरबारी शायर का ये कलाम, शिशिर परखी की मखमली आवाज़ में -
मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक - एक परिचय
‘ज़ौक़’ 1204 हि. तदनुसार 1789 ई. में दिल्ली के एक ग़रीब सिपाही शेख़ मुहम्मद रमज़ान के घर पैदा हुए थे। शेख़ रमज़ान नवाब लुत्फअली खां के नौकर थे और काबुली दरवाज़े के पास रहते थे। शैख़ इब्राहीम इनके इकलौते बेटे थे। बचपन में मुहल्ले के एक अध्यापक हाफ़िज़ गुलाम रसूल के पास पढ़ने के लिए जाते। हाफ़िज़ जी शायर भी थे और मदरसे में भी ‘शे’रो-शायरी का चर्चा होता रहता था, इसी से मियां इब्राहीम की तबीयत भी इधर झुकी। इनके एक सहपाठी मीर काज़िम हुसैन ‘बेक़रार’ भी शायरी करते थे और हाफ़िज जी से इस्लाह लेते थे। मियां इब्राहीम की उनसे दोस्ती थी। एक रोज़ उन्होंने एक ग़ज़ल सुनायी जो मियां इब्राहीम को पसंद आयी। पूछने पर काज़िम हुसैन ने बताया कि हम तो शाह नसीर (उस ज़माने के एक मशहूर शायर) के शागिर्द हो गये हैं और ग़ज़ल उन्हीं की संशोधित की हुई है। चुनांचे इब्राहीम साहब को भी शौक़ पैदा हुआ कि उनके साथ जाकर शाह नसीर के शिष्य हो गए।
लेकिन शाह नसीर ने इनके साथ वैसा सुलूक न किया जैसा बुजुर्ग उस्ताद को करना चाहिए था। मियां इब्राहीम में काव्य-रचना की प्रतिभा प्रकृति-प्रदत्त थी और शीघ्र ही मुशायरों में इनकी ग़जलों की तारीफ़ होने लगी। शाह नसीर को ख़याल हुआ कि शायद शागिर्द उस्ताद से भी आगे बढ़ जाय और उन्होंने न केवल इनकी ओर से बेरुख़ी बरती बल्कि इन्हें निरुत्साहित भी किया। इनकी ग़ज़लों में कभी बेपरवाही से इस्लाह दी और अक्सर बग़ैर इस्लाह के ही बेकार कहकर वापस फेरने लगे। इनके अस्वीकृत शे’रों के मज़मून भी शाह नसीर के पुत्र शाह वजीहुद्दीन ‘मुनीर’ की ग़ज़लों में आने लगे जिससे इन्हें ख़याल हुआ कि उस्ताद इनके विषयों पर शे’र कहकर अपने पुत्र को दे देते हैं। इससे कुछ यह खुद ही असंतुष्ट हुए, कुछ मित्रों ने उस्ताद के ख़िलाफ़ इन्हें उभारा। इसी दशा में एक दिन यह ‘सौदा’ की एक ग़ज़ल पर ग़ज़ल कहकर उस्ताद के पास लेकर गए। उन्होंने नाराज़ होकर ग़ज़ल फेंक दी और कहा ‘‘अब तू मिर्ज़ा रफ़ी सौदा से भी ऊंचा उड़ने लगा ?’’ यह हतोत्साह होकर जामा मस्जिद में आ बैठे। वहां एक बुजुर्ग मीर कल्लू ‘हक़ीर’ के प्रोत्साहन से ग़ज़ल मुशायरे में पढ़ी और खूब वाहवाही लूटी। उस दिन से ‘ज़ौक़’ ने शाह नसीर की शागिर्दी छोड़ दी।
उस्ताद से आज़ाद हो गये तो ख़याल हुआ कि शहर में होने वाली नामवरी को आगे बढ़ाकर शाही किले पहुँचाया जाय। उन दिनों अकबर शाह द्वितीय बादशाह थे। उन्हें कविता से कुछ लगाव न था लेकिन युवराज मिर्ज़ा अबू ज़फ़र (जो बाद में बहादुरशाह द्वितीय के नाम से बादशाह हुए) स्वयं कवि थे और क़िले में अक्सर काव्य-गोष्ठियां कराया करते थे जिनमें उस समय के पुराने-पुराने शायर आते थे। लेकिन मियां इब्राहीम एक ग़रीब सिपाही के बेटे, किसी रईस की ज़मानत के बग़ैर क़िले में कैसे जाने पायें। काफ़ी कोशिश के बाद मीर काज़िम हुसैन की मध्यस्थता से क़िले के मुशायरों में शरीक होने लगे। काज़िम साहब खुद भी उस ज़माने के अच्छे शायरों में समझे जाने लगे थे। उन दिनों शाह नसीर युवराज के कविता-गुरु थे। कुछ दिनों बाद वे दीवान चन्दूलाल के बुलावे पर हैदराबाद चले गए क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह दरबार दिल्ली से कहीं लाभदायक था। उनके बाद मीर काज़िम हुसैन युवराज को इस्लाह देने लगे लेकिन कुछ दिनों बाद वे भी मि. जॉन ऐलफ़िन्सटन के मीर-मुंशी होकर पश्चिम की ओर चले गये। ऐसे ही में एक दिन संयोगवश युवराज ने ‘ज़ौक़’ को (जो अभी बिल्कुल लड़के ही थे) अपनी ग़ज़ल दिखायी। इस्लाह उन्हें इतनी पसंद आयी कि उन्होंने इन्हें अपना कविता गुरु बना लिया और तनख़्वाह भी चार रुपया महीना मुक़र्रर कर दी। इस अल्प वेतन का भी दिलचस्प इतिहास है। बादशाह अकबर शाह अपनी एक बेग़म मुमताज़ से खुश थे और उनके कहने से मिर्ज़ा ज़फ़र को युवराज-पद से अलग करना चाहते थे। अंगरेज़ी अदालत में इसका मुकद्दमा भी चल रहा था। युवराज को उनके नियत 5000 रुपये की बजाय 500 रुपया महीना ही मिलता था। इसी में सारे शाही ठाठ-बाट करने पड़ते थे। उनके मुख़्तारे-आ़म मिर्ज़ा मुग़ल बेग थे इन महानुभाव का काम यह था कि युवराज पर जिसकी कृपा होती थी उसका पत्ता काटने की फ़िक्र में लग जाते थे। चुनांचे इन की मेहरबानी से तनख़्वाह चार रुपये से शुरू हुई और फिर दो बार तरक़्क़ी हुई तो चार से पांच और पांच से सात हो गयी। ‘ज़ौक़’ अगर चाहते तो युवराज से कहकर इस ज़लील तनख़्वाह को क़ायदे की करा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी अपने मालिक से एक शब्द भी नहीं कहा।
‘ज़ौक़’ के पिता ने उन्हें बादशाह से बिगाड़ करने वाले युवराज की इतनी कम तनख़्वाह पर नौकरी करने से मना भी किया लेकिन इन्हें कुछ युवराज की तबियत इतनी भा गई थी कि किसी बात का ख़याल न किया और नौकरी करते रहे। इधर दिल्ली के एक पुराने रईस और मिर्ज़ा ग़ालिब के ससुर नवाब इलाही बख़्श खां ने इन्हें बुलवाया और यद्यपि वे स्वयं बहुत बूढ़े हो चुके थे तथापि इस अल्पायु कवि से अपनी कविताओं में संशोधन कराने लगे। ‘ज़ौक़’ अपने इन दोनों ‘शागिर्दों’ से उम्र और रुतबे में बहुत ही कम थे। साथ ही ख़ानदानी ग़रीबी ने पढ़ने भी ज़्यादा न दिया था। इसलिए यह अपनी उस्तादी क़ायम रखने के लिए खुद ही कविता का जी तोड़कर अभ्यास करने लगे और अपनी जन्मजात प्रतिभा के बल पर इस कला में शीघ्र ही निपुण हो गये। ख़ास तौर पर नवाब साहब की उस्तादी ने, जो हर रंग के शे’र कहते थे, इन्हें हर रंग का उस्ताद बना दिया।
इसी ज़माने में शाह नसीर हैदराबाद से लौटे। (शाह नसीर धनार्जन के लिए तीन बार हैदराबाद गये और फिर दिल्ली के आकर्षण ने उन्हें यहां ला खैंचा। लखनऊ भी दो बार जाकर लौट आये। अंत में चौथी बार की हैदराबाद यात्रा में उनका वहीं देहान्त हुआ।) दिल्ली आकर उन्होंने फिर अपने मुशायरे जारी कराये। अब ‘ज़ौक़’ इनमें शामिल हुए तो शागिर्द की नहीं, प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से शामिल हुए। शाह नसीर ने एक ग़ज़ल लिखी थी जिसकी रदीफ़ थी ‘‘आबो-ख़ाको-बाद’’। उन दिनों मुश्किल रदीफ़ क़ाफ़ियों में पूरे मतलब के साथ और काव्य-परम्परा क़ायम रखते हुए ग़ज़लें कहना ही काव्य-कला का चरमोत्कर्ष समझा जाता था। शाह नसीर ने चुनौती दी कि इस रदीफ़ क़ाफ़िए में कोई ग़ज़ल कह दे तो उसे उस्ताद मान लूं। ‘ज़ौक़’ को तो शाह साहब को नीचा दिखाना था। उन्होंने इस ज़मीन में एक ग़ज़ल और तीन कसीदे कह दिये। शाह साहब ने मुशायरे ही में उस पर अपने शागिर्दों से एतराज करवाये और खुद भी किये लेकिन ‘ज़ौक़’ ने अपने तर्कों से सब को चुप कर दिया। अब ‘ज़ौक़’ की धाक उस्ताद की हैसियत से अच्छी तरह जम गयी। लेकिन इससे यह न समझना चाहिए कि ‘ज़ौक़’ की व्यक्तिगत रूप से भी शाह साहब से अनबन हो गयी थी। दोनों के मैत्री-संबंध अंत तक बने रहे। शाह नसीर की उर्स आदि की दावत में ‘ज़ौक़’ बराबर जाते थे। शाह नसीर अंतिम बार जब हैदराबाद गये तो ‘ज़ौक़’ ने बुढ़ापे के ख़याल से उन्हें वहां जाने से रोकना भी चाहा था।
लेकिन ‘ज़ौक़’ को अपनी कविता की धाक बिठाने से अधिक अपनी कमजोरियों को दूर करने की चिन्ता थी। (बड़प्पन इसी तरह मिलता है।) उन्हें अपने अध्ययन के अभाव की बराबर खटक रहा करती थी। संयोग से अवध के नवाब के मुख्तार राजा साहब राम ने अपने पुत्र को तत्कालीन विद्याओं-इतिहास, तर्कशास्त्र, गणित आदि-में पारंगत करना चाहा और इसके लिए ‘ज़ौक़’ के एक पुराने गुरु मौलवी अब्दुर्रज़ाक को नियुक्त किया। एक दिन ‘ज़ौक़’ भी मौलवी साहब के यहां चले गये। राजा साहब उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि इनसे कहा कि तुम बराबर पढ़ने आया करो। यहां तक कि अगर किसी कारण ‘ज़ौक़’ किसी दिन न आते तो राजा साहब का आदमी उन्हें ढूँढ़ने के लिए भेजा जाता और अगर फिर भी वे न आते तो उस दिन की पढ़ाई स्थगित हो जाती। ‘ज़ौक़’ की क़िस्मत ही ज़ोरदार थी, वर्ना इतने निस्वार्थ सहायक कितनों को मिल पाते हैं।
लेकिन उनकी असली सहायक उनकी जन्मजात प्रतिभा और अध्ययनशीलता थी। कविता-अध्ययन का यह हाल कि पुराने उस्तादों के साढ़े तीन सौ दीवानों को पढ़कर उनका संक्षिप्त संस्करण किया। कविता की बात आने पर वह अपने हर तर्क की पुष्टि में तुरंत फ़ारसी के उस्तादों का कोई शे’र पढ़ देते थे। इतिहास में उनकी गहरी पैठ थी। तफ़सीर (कुरान की व्याख्या) में वे पारंगत थे, विशेषतः सूफी-दर्शन में उनका अध्ययन बहुत गहरा था। रमल और ज्योतिष में भी उन्हें अच्छा-खासा दख़ल था और उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही निकलती थीं। स्वप्न-फल बिल्कुल सही बताते थे। कुछ दिनों संगीत का भी अभ्यास किया था और कुछ तिब्ब (यूनानी चिकित्सा-शास्त्र) भी सीखी थी। धार्मिक तर्कशास्त्र (मंतक़) और गणित में भी वे पटु थे। उनके इस बहुमुखी अध्ययन का पता अक्सर उनके क़सीदों से चलता है जिनमें वे विभिन्न विद्याओं के पारिभाषिक शब्दों के इतने हवाले देते हैं कि कोई विद्वान ही उनका आनंद लेने में समर्थ हो सकता है। उर्दू कवियों में इस कोटि के विद्वान कम ही हुए हैं।
किन्तु उनकी पूरी प्रतिभा काव्य-क्षेत्र ही में दिखाई देती थी 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बादशाह अकबर शाह के दरबार में एक क़सीदा सुनाया। इसमें फ़ारसी काव्य में वर्णित समस्त अलंकार तो थे ही, साथ ही विभिन्न विद्याओं की भी अच्छी जानकारी दर्शाई गई थी। इसके, अतिरिक्त इसमें एक ही ज़मीन में 18 विभिन्न भाषाओं में शे’र कहकर शामिल किये गए थे। इस क़सीदे का पहला शे’र यह है :
जब कि सरतानो-असद मेहर का ठहरा मसकन
आबो-ऐलोला हुए नश्वो-नुमाए-गुलशन
इस पर उन्हें ‘ख़ाक़ानी-ए-हिन्द’ का ख़िताब मिला। ख़ाकानी फ़ारसी भाषा का बहुत मशहूर क़सीदा कहने वाला शायर था। 19 वर्ष की अवस्था में यह ख़िताब पाना कमाल है।
36 वर्ष की अवस्था में समस्त पापों से तौबा की और इसकी तारीख़ कही:
ऐ ज़ौक़ बिगो सह बार तौबा।’’ यानी ‘‘ऐ ज़ौक़ तीन बार तौबा कह।
भगवान ने ‘ज़ौक़’ को बुद्धि और मृदु स्वभाव देने में जो दानशीलता दिखायी थी, शारीरिक व्यक्तित्व देने में उतनी ही बेपरवाही बरती। उनका क़द साधारण से कुछ कम ही था और रंगत सांवली। चेहरे पर चेचक के दाग़ बहुतायत से थे। खुद कहते थे कि मुझे नौ बार चेचक निकली थी किन्तु आंखें चमकती हुई थीं। चेहरे का नक़्शा खड़ा-खड़ा था। बदन में बहुत फुरती थी, बहुत तेज़ चलते थे। कपड़े अक्सर सफ़ेद पहनते थे, वह उन पर भले ही लगते थे। आवाज़ ऊंची और सुरीली थी। मुशायरे में ग़जल पढ़ते तो आवाज़ गूंजकर रह जाती थी। उनके पढ़ने का तर्ज़ भी बड़ा अच्छा था। हमेशा अपनी ग़ज़ल खुद ही पढ़ते थे, किसी और से कभी नहीं पढ़वाते थे।
उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। जितनी विद्याएं और उर्दू फ़ारसी की जितनी कविता-पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थीं, उन्हें वे अपने मस्तिष्क में इस प्रकार सुरक्षित रखे हुए थे कि हवाला देने के लिए पुस्तकों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपनी स्मरण-शक्ति के बल पर हवाले देते चले जाते थे। सही बात तो यह है कि इतनी विद्याओं का सीखना भी अति तीक्ष्ण ग्रहण-शक्ति और स्मरण-शक्ति के बग़ैर संभव नहीं था।
बहादुरशाह बादशाह हुए तो उनके मुख़्तार मिर्ज़ा मुग़ल बेग मंत्री हुए। उन्होंने अपना पूरा कुनबा क़िले में भर लिया किन्तु उस्ताद की तनख़्वाह सात रुपये से बढ़ी तो तीस रुपया महीना हो गई। ‘ज़ौक़’ को यह बेक़दरी बहुत बुरी मालूम होती थी। लेकिन स्वभाव में संतोष बहुत था। कभी बादशाह से इसकी शिकायत नहीं की। उन्हें खुद क्या ख़बर होती कि किसे कितना मिल रहा है। ‘ज़ौक़’ ग़रीबी के दिन काटते रहे।
अंत में पाप का घड़ा फूटा। मिर्ज़ा मुग़ल बेग और उनका सारा कुनबा क़िले से निकाला गया। ‘ज़ौक़’ की तनख़्वाह बढ़कर सौ रुपया महीना हो गई। यद्यपि यह तनख़्वाह भी उनकी योग्यता को देखते हुए कुछ न थी और हैदराबाद से दीवान चन्दूलाल ने ख़िलअ़त और 500 रुपये भेजकर इन्हें बुलाया लेकिन यह ‘ज़फ़र’ का दामन छोड़कर कहीं न गये।
तनख़्वाह के अलावा ईद-बक़रीद पर इनाम भी मिला करते थे। अंतिम काल में उन्होंने बादशाह के बीमारी से अच्छे होने पर एक कंसीदा, ‘‘वाहवा, क्या मोतदिल है बाग़े-आ़लम की हवा’’ पढ़ा। इस पर उन्हें ख़िलअ़त, ख़ान बहादुरी का ख़िताब और चांदी के हौदे के साथ एक हाथी मिला। फिर उन्होंने एक क़सीदा कहा, ‘‘शब को मैं अपने सरे-बिस्तरे-ख़्वाबे-राहत।’’ इस पर उन्हें एक गांव जागीर में मिला।
अंत में इस कमाल के उस्ताद ने 1271 हिजरी (1854 ई.) में सत्रह दिन बीमार रहकर परलोक गमन किया। मरने के तीन घंटे पहले यह शे’र कहा था:
कहते हैं ‘ज़ौक़’ आज जहां से गुज़र गया
क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़रत करे

ज़ौक़ और शाही फरमाईशों के दिलचस्प किस्से
मुग़लिया सल्तनत के आख़िरी चिराग़ बहादुरशाह द्वितीय के शहज़ादे जवांबख़्त की शादी है। ‘ग़ालिब’ एक सेहरा पेश करते हैं जिसका मक़तअ़ है :
हम सुखन-फ़हम हैं ‘ग़ालिब’ के तरफ़दार नहीं
देखें इस सेहरे से कह दे कोई बेहतर सेहरा
बादशाह को ख़याल होता है कि ‘ग़ालिब’ उनकी सुख़नफ़हमी पर चोट कर रहे हैं कि मुझे जैसे बाकमाल शायर के रहते हुए ‘ज़ौक़’ को उस्ताद किया है। फ़ौरन ही उस्ताद बुलाये जाते हैं और हुक्म होता है कि जवाब में सेहरा लिखो और इसी वक़्त लिखो। ‘ज़ौक़’ बेचारे वहीं बैठ जाते हैं और जवाब में सेहरा लिख देते हैं। बादशाह की उस्तादी भी पकड़बुलावे की नौकरी है।
लेकिन शायद आप यह कहें कि इसमें ज़बर्दस्ती की क्या बात है, ‘ज़ौक़’ ने तो खुशी से अपने ऊपर की गयी ‘चोट’ का जवाब दिया होगा। बहुत अच्छा, मान लिया। लेकिन इस पर क्या कहिएगा-बरसात का मौसम है, बादशाह के साथ युवराज मिर्ज़ा फ़ख़रू भी कुतुब साहब के पास चांदनी रात में तालाब के किनारे सैर कर रहे हैं। ‘ज़ौक़’ भी खड़े हैं। ‘मिर्ज़ा’ फ़ख़रू भी ‘ज़ौक’ के शागिर्द हैं। उनकी ज़बान से मिसरा निकलता है-‘‘चांदनी देखे अगर वह महजबीं तालाब पर’’, और साथ ही हुक्म होता है कि उस्ताद, इस पर मिसरा लगाना। उस्ताद फ़ौरन मिसरा लगाते हैं, ‘‘ताबे-अक़्से-रूख़ से पानी फेर दे महताब पर।’’
बादशाह की उस्तादी ‘ज़ौक़’ को किस क़दर महंगी पड़ी थी, यह उनके शागिर्द मौलाना मुहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़बानी सुनिए:
‘‘वह अपनी ग़ज़ल खुद बादशाह को न सुनाते थे। अगर किसी तरह उस तक पहुंच जाती तो वह इसी ग़ज़ल पर खुद ग़ज़ल कहता था। अब अगर नयी ग़ज़ल कह कर दें और वह अपनी ग़ज़ल से पस्त हो तो बादशाह भी बच्चा न था, 70 बरस का सुख़न-फ़हन था। अगर उससे चुस्त कहें तो अपने कहे को आप मिटाना भी कुछ आसान काम नहीं। नाचार अपनी ग़ज़ल में उनका तख़ल्लुस डालकर दे देते थे। बादशाह को बड़ा ख़याल रहता था कि वह अपनी किसी चीज़ पर ज़ोर-तबअ़ न ख़र्च करें। जब उनके शौक़े-तबअ़ को किसी तरफ़ मुतवज्जह देखता जो बराबर ग़ज़लों का तार बांध देता कि तो कुछ जोशे-तबअ़ हो इधर ही आ जाय।’’
शाही फ़रमायशों की कोई हद न थी। किसी चूरन वाले की कोई कड़ी पसंद आयी और उस्ताद को पूरा लटका लिखने का हुक्म हुआ। किसी फ़क़ीर की आवाज़ हुजूर को भा गयी है और उस्ताद पूरा दादरा बना रहे हैं। टप्पे, ठुमरियां, होलियां, गीत भी हज़ारों कहे और बादशाह को भेंट किये। खुद भी झुंझला कर एक बार कह दिया :
ज़ौक मुरत्तिब क्योंकि हो दीवां शिकवाए-फुरसत किससे करें
बांधे हमने अपने गले में आप ‘ज़फ़र’ के झगड़े हैं
और एक वर्तमान आलोचक हैं कि ‘ज़ौक़’ का नाम महाकवियों की सूची में रखने में हिचकते हैं। ‘ग़ालिब’, ‘मोमिन’, ‘आतिश’, ‘नज़ीर’ सभी इस ज़माने के आलोचकों के प्रिय कवि हैं, ‘ज़ौक़’ की लोकप्रियता, मालूम होता है पिछली पीढ़ी के साथ तिरोहित हो गई। ‘ग़ालिब’, ‘मोमिन’ आदि के कमाल पर जिसे शक हो उस पर सौ लानतें, लेकिन उन उस्तादों की प्रशस्ति के लिए ‘ज़ौक़’ या ‘दाग़’ के अपने कमाल की ओर से उपेक्षा बरतना भी निष्पक्ष आलोचना नहीं कही जा सकती। अगर और बातों को छोड़ दिया जाय तो भी सिर्फ़ इतनी सी ही बात ‘ज़ौक़’ को अमर कर देने के लिए काफ़ी है कि वे उम्र भर अपने कांधे पर सल्तनते-मुग़लिया के भारी-भरकम ताज़िए बहादुर शाह ‘ज़फ़र’ को ढोये रहे और साथ ही साहित्य को स्पष्टतः कुछ ऐसी चीज़ें भी दे गये जिनका आज की अस्थिर मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में चाहे कुछ महत्व न मालूम हो किन्तु जिनमें निस्सन्देह कुछ स्थायी मूल्य निहित हैं जिससे किसी ज़माने में इन्कार नहीं किया जा सकता।
लेकिन ‘ज़ौक़’ के काव्य के इन स्थायी तत्वों की व्याख्या के पहले उनके बारे में फैली हुई कुछ भ्रांतियों का निवारण आवश्यक मालूम होता है। पहली बात तो यह है कि समकालीन होने के लिहाज़ से उन्हें ‘ग़ालिब’ का प्रतिद्वंद्वी समझ लिया जाता है और चूंकि यह शताब्दी ‘ग़ालिब’ के उपासकों की है इसलिए ‘ज़ौक़’ से लोग खामखाह ख़ार खाये बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि समकालीन महाकवियों में कुछ न कुछ प्रतिद्वंद्विता होती ही है और ‘ज़ौक़’ ने भी कभी-कभी मिर्ज़ा ‘ग़ालिब’ की छेड़-छाड़ की बादशाह से शिकायत कर दी थी, लेकिन इन दोनों की प्रतिद्वंद्विता में न तो वह भद्दापन था जो ‘इंशा’ और ‘मसहफ़ी’ की प्रतिद्वंद्विता में था, न इतनी कटुता जो ‘मीर’ और ‘सौदा’ में-बावजूद इसके कि ‘मीर’ और ‘सौदा’ एक-दूसरे के कमाल के क़ायल थे-कभी-कभी दिखाई देती है। ‘ज़ौक़’ और ‘ग़ालिब’ में ‘दाग़’ और ‘अमीर’ की भांति समकालीन होते हुए भी प्रतिद्वंद्विता का अभाव और परस्पर प्रेम भी नहीं दिखाई देता, वास्तविकता यह है कि ‘ज़ौक़’ और ‘ग़ालिब’ दोनों ने इस बात को महसूस कर लिया था कि उनकी प्रतिद्वंद्विता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ‘ग़ालिब’ नयी भाव-भूमियों को अपनाने में दक्ष थे और वर्णन-सौंदर्य की ओर से उदासीन; ‘ज़ौक़’ का कमाल वर्णन-सौंदर्य में था और भावना के क्षेत्र में बुजुर्गों की देन ही को काफ़ी समझते थे। प्रतिद्वंद्विता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था।
साथ ही जैसा कि हर ज़माने के समकालीन महाकवि एक दूसरे के कमाल के क़ायल होते हैं, यह दोनों बुजुर्ग भी एक-दूसरे के प्रशंसक थे। ‘ग़ालिब’ तो बहते दरिया थे, उनकी ईमानदारी का क्या कहना !जैसा की हमने पिछली पोस्ट में ज़िक्र किया था कि ‘मोमिन’ के इस शेर के बदले में :
तुम मेरे पास होते हो गोया
जब कोई दूसरा नहीं होता।
-‘ग़ालिब’ अपना पूरा दीवान देने को तैयार थे। ‘ज़ौक़’ के भी वे प्रशंसक थे और अपने एक पत्र में उन्होंने ‘ज़ौक़’ के इस शे’र की प्रशंसा की है :
अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे
मर गये पर न लगा जी तो किधर जायेंगे।
और उधर ‘ज़ौक़’ भी मुंह-देखी में नहीं बल्कि अपने दोस्तों और शागिर्दों मैं बैठकर कहा करते थे कि मिर्ज़ा (ग़ालिब) को खुद अपने अच्छे शे’रों का पता नहीं है और उनका यह शे’र सुनाया करते थे:
दरियाए-मआ़सी1 तुनुक-आबी से हुआ खुश्क
मेरा सरे-दामन भी अभी तक न हुआ था।
मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान आलोचकों की निगाहें कहां तक इस शे’र की गहराई को देख सकी हैं लेकिन मुझे खुद मिर्ज़ा का यह शे’र उनके सारे दीवान से भारी मालूम होता है और मैं ‘ज़ौक़’ की परिष्कृत रुचि का क़ायल हो गया हूं जिन्होंने उस आकारवादी (Formalistic) युग में और स्वयं आकारवाद के एक प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी इस शे’र को ‘ग़ालिब’ के दीवान के घने जंगल में से छांट लिया।
‘ज़ौक़’ के मुकाबले में ‘ग़ालिब’ को ऊंचा उठाने में कुछ लोग दो बातों पर ख़ास तौर पर ज़ोर देते हैं। एक तो ‘ग़ालिब’ की निर्धनता में भी कायम रहने वाली मस्ती और दूसरे उनका आत्म-सम्मान। ‘ग़ालिब’ में यह दोनों बातें थीं इससे किसी को इनकार न होना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं लोग यह क्यों नहीं देख पाये कि ‘ज़ौक़’ में ये दोनों गुण ‘ग़ालिब’ से कम नहीं, कुछ
अधिक ही थे। हां, यह बात ज़रूर है कि ‘ग़ालिब’ ने अपने पत्रों में इन गुणों का स्वयं ही प्रदर्शन कर दिया है, ‘ज़ौक़’ बिल्कुल खामोश हैं और हमें खुद मेहनत करके उनके व्यक्तित्व की गहराई को जांचना पड़ेगा।
---प्रकाश पंडित की पुस्तक “ज़ौक़ और उनकी शायरी” से साभार
ghazal - laaye hayaat...
singer/composer - shishir parkhie
album - ahtaraam
tribute to the legend poets/shayar series part # 02




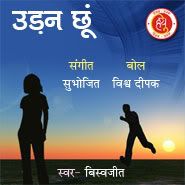


 संस्कार गीतों पर एक विशेष शृंखला
संस्कार गीतों पर एक विशेष शृंखला मन जाने - विवधताओं से भरी अल्बम
मन जाने - विवधताओं से भरी अल्बम








 लता मंगेशकर जब मिली आवाज़ के श्रोताओं से
लता मंगेशकर जब मिली आवाज़ के श्रोताओं से द रिटर्न ऑफ आलम आरा प्रोजेक्ट एक कोशिश है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म के गीत संगीत को फिर से रिवाईव करने की, सहयोग दें, और हमारी इस नेक कोशिश का हिस्सा बनें
द रिटर्न ऑफ आलम आरा प्रोजेक्ट एक कोशिश है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म के गीत संगीत को फिर से रिवाईव करने की, सहयोग दें, और हमारी इस नेक कोशिश का हिस्सा बनें 

 सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन यानी इंडस्ट्री के दाद्दु पर एक विशेष शृंखला जिसके माध्यम हम सलाम कर रहे हैं फिल्म संगीत जगत में, इस अदभुत कलाकार के सुर्रिले योगदान को
सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन यानी इंडस्ट्री के दाद्दु पर एक विशेष शृंखला जिसके माध्यम हम सलाम कर रहे हैं फिल्म संगीत जगत में, इस अदभुत कलाकार के सुर्रिले योगदान को लोरियों की मधुरता स्त्री स्वर के माम्तत्व से मिलकर और भी दिव्य हो जाती है. पर फिल्मों में यदा कदा ऐसी परिस्थियों भी आई है जब पुरुष स्वरों ने लोरियों को अपनी सहजता प्रदान की है. पुरुष स्वरों की दस चुनी हुई लोरियाँ लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं ओल्ड इस गोल्ड में इन दिनों
लोरियों की मधुरता स्त्री स्वर के माम्तत्व से मिलकर और भी दिव्य हो जाती है. पर फिल्मों में यदा कदा ऐसी परिस्थियों भी आई है जब पुरुष स्वरों ने लोरियों को अपनी सहजता प्रदान की है. पुरुष स्वरों की दस चुनी हुई लोरियाँ लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं ओल्ड इस गोल्ड में इन दिनों 

 शक्ति के बिना धैर्य ऐसे ही है जैसे बिना बत्ती के मोम।
शक्ति के बिना धैर्य ऐसे ही है जैसे बिना बत्ती के मोम।



आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
3 श्रोताओं का कहना है :
बहुत बढ़िया संकलन .ग़ज़ल भी बहुत सुंदर और मधुर है.
ग़ज़ल तो नायाब है ही, साथ में जो जानकारी दी गई है, वो अनमोल है। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति है आवाज़ की।
पारखी नज़रों से बच सके हीरा कैसे,
शिशिर की धूप खुशगवार हो तो ज़ौक मिले।
आपकी आवाज़ और आपके आलेख दोनों का मुरीद हो गया हूँ।
अब तक ज़ौक का बस नाम जानता था, खुशी है कि अब उनके बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ।
शुक्रिया एवं बधाईयाँ।
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)