महफ़िल-ए-ग़ज़ल #९७
नाज़ है गुल को नज़ाक़त पै चमन में ऐ ‘ज़ौक़’,
इसने देखे ही नहीं नाज़-ओ-नज़ाक़त वाले
इस तपिश का है मज़ा दिल ही को हासिल होता
काश, मैं इश्क़ में सर-ता-ब-क़दम दिल होता
यूँ तो इश्क़ और शायर/शायरी में चोली-दामन का साथ होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शायर होते हैं जो इश्क़ को बखूबी समझते हैं और हर शेर लिखने से पहले स्याही को इश्क़ में डुबोते चलते हैं। ऐसे शायरों का लिखा पढने में दिल को जो सुकूं मिलता है, वह लफ़्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। ज़ौक़ वैसे हीं एक शायर थे। जितनी आसानी ने उन्होंने "सर-ता-ब-कदम" दिल होने की बात कही है या फिर यह कहा है कि गुलशन के फूलों को जो अपनी नज़ाकत पे नाज़ है, उन्हें यह मालूम नहीं कि यह नाज़-ओ-नज़ाकत उनसे बढकर भी कहीं और मौजूद है .. ये सारे बिंब पढने में बड़े हीं आम मालूम होते हैं ,लेकिन लिखने वाले को हीं पता होता है कि कुछ आम लिखना कितना खास होता है। मैंने ज़ौक़ की बहुत सारी ग़ज़लें पढी हैं.. उनकी हर ग़ज़ल और ग़ज़ल का हर शेर इस बात की गवाही देता है कि यह शायर यकीनन कुछ खास रहा है। फिर भी न जाने क्यों, हमने इन्हें भुला दिया है या फिर हम इन्हें भुलाए जा रहे हैं। इस गु़स्ताखी या कहिए इस गलती की एक हीं वज़ह है और वह है ग़ालिब की हद से बढकर भक्ति। अब होता है ये है कि जो भी सुखनसाज़ या सुखन की कद्र करने वाला ग़ालिब को अपना गुरू मानने लगता है, उसके लिए यक-ब-यक ज़ौक़ दुश्मन हो जाते हैं। उन लोगों को यह लगने लगता है कि ज़ौक़ की हीं वज़ह से ग़ालिब को इतने दु:ख सहने पड़े थे, इसलिए ज़ौक़ निहायत हीं घटिया इंसान थे। इस सोच का जहन में आना होता है कि वे सब ज़ौक़ की शायरी से तौबा करने लगते हैं। मुझे ऐसी सोच वाले इंसानों पे तरस आता है। शायर को उसकी शायरी से मापिए, ना कि उसके पद या ओहदे से। ज़ौक़ ज़फ़र के उस्ताद थे और उनके दरबार में रहा करते थे.. अगर दरबार में रहना गलत है तो फिर ग़ालिब ने भी तो दरबार में रहने के लिए हाथ-पाँव मारे थे। तब तो उन्हें भी बुरा कहा जाना चाहिए, पथभ्रष्ट कहा जाना चाहिए। सिर्फ़ ग़ालिब और ज़ौक़ के समकालीन होने के कारण ज़ौक़ से नाक-भौं सिकोड़ना तो सही नहीं। मुझे मालूम है कि हममें से भी कई या तो ज़ौक़ को जानते हीं नहीं होंगे या फिर जानकर भी अनजान रहना हीं पसंद करते होंगे। अपने वैसे मित्रों के लिए मैं "प्रकाश पंडित" जी के खजाने से "ज़ौक़" से ताल्लुक रखने वाले कुछ मोती चुनकर लाया हूँ। इसे पढने के बाद यकीनन हीं ज़ौक़ के प्रति बरसों में बने आपके विचार बदलेंगें।
प्रकाश जी लिखते हैं:
उर्दू शायरी में ‘ज़ौक़’ का अपना खास स्थान है। वे शायरी के उस्ताद माने जाते थे। आखिरी बादशाह बहादुरशाह ज़फ़र के दरबार में शाही शायर भी थे।
बादशाह की उस्तादी ‘ज़ौक़’ को किस क़दर महंगी पड़ी थी, यह उनके शागिर्द मौलाना मुहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़बानी सुनिए:
"वह अपनी ग़ज़ल खुद बादशाह को न सुनाते थे। अगर किसी तरह उस तक पहुंच जाती तो वह इसी ग़ज़ल पर खुद ग़ज़ल कहता था। अब अगर नयी ग़ज़ल कह कर दें और वह अपनी ग़ज़ल से पस्त हो तो बादशाह भी बच्चा न था, 70 बरस का सुख़न-फ़हन था। अगर उससे चुस्त कहें तो अपने कहे को आप मिटाना भी कुछ आसान काम नहीं। नाचार अपनी ग़ज़ल में उनका तख़ल्लुस डालकर दे देते थे। बादशाह को बड़ा ख़याल रहता था कि वह अपनी किसी चीज़ पर ज़ोर-तबअ़ न ख़र्च करें। जब उनके शौक़े-तबअ़ को किसी तरफ़ मुतवज्जह देखता जो बराबर ग़ज़लों का तार बांध देता कि तो कुछ जोशे-तबअ़ हो इधर ही आ जाय।"
शाही फ़रमायशों की कोई हद न थी। किसी चूरन वाले की कोई कड़ी पसंद आयी और उस्ताद को पूरा लटका लिखने का हुक्म हुआ। किसी फ़क़ीर की आवाज़ हुजूर को भा गयी है और उस्ताद पूरा दादरा बना रहे हैं। टप्पे, ठुमरियां, होलियां, गीत भी हज़ारों कहे और बादशाह को भेंट किये। खुद भी झुंझला कर एक बार कह दिया :
ज़ौक मुरत्तिब क्योंकि हो दीवां शिकवाए-फुरसत किससे करें
बांधे हमने अपने गले में आप ‘ज़फ़र’ के झगड़े हैं
"ज़ौक़" के काव्य के स्थायी तत्वों की व्याख्या के पहले उनके बारे में फैली हुई कुछ भ्रांतियों का निवारण आवश्यक मालूम होता है। पहली बात तो यह है कि समकालीन होने के लिहाज़ से उन्हें ‘ग़ालिब’ का प्रतिद्वंद्वी समझ लिया जाता है और चूंकि यह शताब्दी ‘ग़ालिब’ के उपासकों की है इसलिए ‘ज़ौक़’ से लोग खामखाह ख़ार खाये बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि समकालीन महाकवियों में कुछ न कुछ प्रतिद्वंद्विता होती ही है और ‘ज़ौक़’ ने भी कभी-कभी मिर्ज़ा ‘ग़ालिब’ की छेड़-छाड़ की बादशाह से शिकायत कर दी थी, लेकिन इन दोनों की प्रतिद्वंद्विता में न तो वह भद्दापन था जो ‘इंशा’ और ‘मसहफ़ी’ की प्रतिद्वंद्विता में था, न इतनी कटुता जो ‘मीर’ और ‘सौदा’ में कभी-कभी दिखाई देती है। असल में उनके बीच प्रतिद्वंद्विता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। ‘ग़ालिब’ नयी भाव-भूमियों को अपनाने में दक्ष थे और वर्णन-सौंदर्य की ओर से उदासीन; ‘ज़ौक़’ का कमाल वर्णन-सौंदर्य में था और भावना के क्षेत्र में बुजुर्गों की देन ही को काफ़ी समझते थे। जैसा कि हर ज़माने के समकालीन महाकवि एक दूसरे के कमाल के क़ायल होते हैं, यह दोनों बुजुर्ग भी एक-दूसरे के प्रशंसक थे। ग़ालिब ‘ज़ौक़’ के प्रशंसक थे और अपने एक पत्र में उन्होंने ‘ज़ौक़’ के इस शे’र की प्रशंसा की है :
अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे
मर गये पर न लगा जी तो किधर जायेंगे।
और उधर ‘ज़ौक़’ भी मुंह-देखी में नहीं बल्कि अपने दोस्तों और शागिर्दों मैं बैठकर कहा करते थे कि मिर्ज़ा (ग़ालिब) को खुद अपने अच्छे शे’रों का पता नहीं है और उनका यह शे’र सुनाया करते थे:
दरियाए-मआ़सी तुनुक-आबी से हुआ खुश्क
मेरा सरे-दामन भी अभी तक न हुआ था।
ज़ौक़ की असली सहायक उनकी जन्मजात प्रतिभा और अध्ययनशीलता थी। कविता-अध्ययन का यह हाल कि पुराने उस्तादों के साढ़े तीन सौ दीवानों को पढ़कर उनका संक्षिप्त संस्करण किया। कविता की बात आने पर वह अपने हर तर्क की पुष्टि में तुरंत फ़ारसी के उस्तादों का कोई शे’र पढ़ देते थे। इतिहास में उनकी गहरी पैठ थी। तफ़सीर (कुरान की व्याख्या) में वे पारंगत थे, विशेषतः सूफी-दर्शन में उनका अध्ययन बहुत गहरा था। रमल और ज्योतिष में भी उन्हें अच्छा-खासा दख़ल था और उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही निकलती थीं। स्वप्न-फल बिल्कुल सही बताते थे। कुछ दिनों संगीत का भी अभ्यास किया था और कुछ तिब्ब (यूनानी चिकित्सा-शास्त्र) भी सीखी थी। धार्मिक तर्कशास्त्र (मंतक़) और गणित में भी वे पटु थे। उनके इस बहुमुखी अध्ययन का पता अक्सर उनके क़सीदों से चलता है जिनमें वे विभिन्न विद्याओं के पारिभाषिक शब्दों के इतने हवाले देते हैं कि कोई विद्वान ही उनका आनंद लेने में समर्थ हो सकता है। उर्दू कवियों में इस कोटि के विद्वान कम ही हुए हैं।
‘ज़ौक़’ १२०४ हि. तदनुसार १७८९ ई. में दिल्ली के एक ग़रीब सिपाही शेख़ मुहम्मद रमज़ान के घर पैदा हुए थे। शेख़ रमज़ान नवाब लुत्फअली खां के नौकर थे। शेख़ इब्राहीम (ज़ौक़ का असल नाम) इनके इकलौते बेटे थे। इस कमाल के उस्ताद ने १२७१ हिजरी (१८५४ ई.) में सत्रह दिन बीमार रहकर परलोक गमन किया। मरने के तीन घंटे पहले यह शे’र कहा था:
कहते हैं ‘ज़ौक़’ आज जहां से गुज़र गया
क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़रत करे
ग़ालिब और ज़ौक़ के बीच शायराना नोंक-झोंक और हँसी-मज़ाक के कई सारे किस्से मक़बूल हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने यह वाक्या ग़ालिब के लिए सजी महफ़िल में सुनाया था या नहीं, अगर सुनाया हो, तब भी दुहराए देता हूँ। बात एक गोष्ठी की है । मिर्ज़ा ग़ालिब मशहूर शायर मीर तक़ी मीर की तारीफ़ में कसीदे गढ़ रहे थे । शेख इब्राहीम ‘जौक’ भी वहीं मौज़ूद थे । ग़ालिब द्वारा मीर की तारीफ़ सुनकर वे बैचेन हो उठे । वे सौदा नामक शायर को श्रेष्ठ बताने लगे । मिर्ज़ा ने झट से चोट की- “मैं तो आपको मीरी समझता था मगर अब जाकर मालूम हुआ कि आप तो सौदाई हैं ।” यहाँ मीरी और सौदाई दोनों में श्लेष है । मीरी का मायने मीर का समर्थक होता है और नेता या आगे चलने वाला भी । इसी तरह सौदाई का पहला अर्थ है सौदा या अनुयायी, दूसरा है- पागल।
ज़ौक़ कितने सौदाई थे या फिर कितने मीरी... इसका निर्धारण हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके लिखे कुछ शेरों को पढकर और उन्हें गुनकर अपने इल्म में थोड़ी बढोतरी तो कर हीं सकते हैं:
आँखें मेरी तलवों से मल जाए तो अच्छा
है हसरत-ए-पा-बोस निकल जाए तो अच्छा
ग़ुंचा हंसता तेरे आगे है जो गुस्ताख़ी से
चटखना मुंह पे वहीं बाद-सहर देती है
आदमीयत और शै है, इल्म है कुछ और शै
कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवाँ ही रहा
वाँ से याँ आये थे ऐ 'ज़ौक़' तो क्या लाये थे
याँ से तो जायेंगे हम लाख तमन्ना लेकर
चलिए अब इन शेरों के बाद उस मुद्दे पर आते हैं, जिसके लिए हमने महफ़िल सजाई है। जानकारियाँ देना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन ग़ज़ल सुनना/सुनवाना तो हमारी ज़िंदगी है.. फ़र्ज़ के मामले में थोड़ा-बहुत इधर-उधर हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से हिली तो खेल खत्म.. है ना? तो आईये.. लगे हाथों हम आज की ग़ज़ल से रूबरू हो लें। आज हम जो ग़ज़ल लेकर महफ़िल में हाज़िर हुए हैं उसे ग़ज़ल-गायिकी की बेताज बेगम "बेगम अख्तर" की आवाज़ नसीब हुई है। इतना कह देने के बाद क्या कुछ और भी कहना बचा रह जाता है। नहीं ना? इसलिए बिना कुछ देर किए, इस ग़ज़ल का लुत्फ़ उठाया जाए:
लायी हयात, आये, क़ज़ा ले चली, चले
अपनी ख़ुशी न आये न अपनी ख़ुशी चले
बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे
पर क्या करें जो काम न बे-दिल्लगी चले
कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बद-क़िमार
जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले
हो उम्रे-ख़िज़्र भी तो भी कहेंगे ब-वक़्ते-मर्ग
हम क्या रहे यहाँ अभी आये अभी चले
दुनिया ने किसका राहे-फ़ना में दिया है साथ
तुम भी चले चलो युँ ही जब तक चली चले
नाज़ाँ न हो ख़िरद पे जो होना है वो ही हो
दानिशतेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले
जा कि हवा-ए-शौक़ में हैं इस चमन से 'ज़ौक़'
अपनी ___ से बादे-सबा अब कहीं चले
वैसे तो हम एक महफ़िल में एक हीं गुलुकार की आवाज़ में ग़ज़ल सुनवाते हैं। लेकिन इस ग़ज़ल की मुझे दो रिकार्डिंग्स हासिल हुई थी.. एक बेग़म अख्तर की और एक कुंदन लाल सहगल की। इन दोनों में से मैं किसे रखूँ और किसे छाटूँ, मैं यह निर्धारित नहीं कर पाया। इसलिए बेगम की आवाज़ में ग़ज़ल सुनवा देने के बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं "सहगल" साहब की बेमिसाल आवाज़ में यही ग़ज़ल एक बार फिर:
चलिए अब आपकी बारी है महफ़िल में रंग ज़माने की... ऊपर जो गज़ल हमने पेश की है, उसके एक शेर में कोई एक शब्द गायब है। आपको उस गज़ल को सुनकर सही शब्द की शिनाख्त करनी है और साथ ही पेश करना है एक ऐसा शेर जिसके किसी भी एक मिसरे में वही खास शब्द आता हो. सही शब्द वाले शेर ही शामिल किये जायेंगें, तो जेहन पे जोर डालिए और बूझिये ये पहेली!
इरशाद ....
पिछली महफिल के साथी -
पिछली महफिल का सही शब्द था "उम्र" और शेर कुछ यूँ था-
आशिक़ तो मुर्दा है हमेशा जी उठता है देखे उसे
यार के आ जाने को यकायक उम्र दो बारा जाने है
इस शब्द पर ये सारे शेर महफ़िल में कहे गए:
आह को चाहिये इक उम्र असर होते तक
कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होते तक (ग़ालिब)
सर्द रातों की स्याही को चुराकर हमने
उम्र यूँ काटी तेरे शहर में आकर हमने (आशीष जी)
उम्रभर तलाशा था हमने जिस हंसी को
आज वो खुद की ही दीवानगी पे आई है (अवनींद्र जी)
उनके बच्चे भी सोये हैं भूखे
जिनकी उम्र गुजरी है रोटियाँ बनाने में (नीलम जी की प्रस्तुति.. शायर का पता नहीं)
उम्र-ए-दराज़ माँग के लाए थे चार दिन
दो आरज़ू में कट गए, दो इन्तज़ार में । (बहादुर शाह ज़फ़र)
ता-उम्र ढूंढता रहा मंजिल मैं इश्क़ की,
अंजाम ये कि गर्द-ए-सफर लेके आ गया। (सुदर्शन फ़ाकिर)
उम्र हो गई तुम्हें पहचानने में ,
अभी तक न जान पाई हमदम मेरे ! (मंजु जी)
दिल उदास है यूँ ही कोई पैगाम ही लिख दो
अपना नाम ना लिखो तो बेनाम ही लिख दो
मेरी किस्मत में गम-ए-तन्हाई है लेकिन
पूरी उम्र ना सही एक शाम ही लिख दो. (शन्नो जी की पेशकश.. शायर का पता नहीं)
उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं
हर शब्-ए-ग़म की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं (ख़ामोश देहलवी) .. नीलम जी, आपके शायर का नाम गलत है।
पिछली महफ़िल की शान बने आशीष जी। इस उपलब्धि के लिए आपको ढेरों बधाईयाँ। मुझे पिछली महफ़िल इसलिए बेहद पसंद आई क्योंकि उस महफ़िल में अपने सारे मित्र मौजूद थे, बस सीमा जी को छोड़कर। न जाने वो किधर गायब हो गई हैं। सीमा जी, आप अगर मेरी यह टिप्पणी पढ रही हैं, तो आज की महफ़िल में टिप्पणी देना न भूलिएगा :) मनु जी, आपको ग़ज़ल पढने में अच्छी लगी, लेकिन सुनने में नहीं। चलिए हमारी आधी मेहनत तो सफल हुई। जहाँ तक सुनने-सुनाने का प्रश्न है और गुलुकार के चयन का सवाल है तो अगर मैं चाहता तो मेहदी हसन साहब या फिर गुलाम अली साहब की आवाज़ में यह ग़ज़ल महफ़िल में पेश करता, लेकिन इनकी आवाज़ों में आपने "पत्ता-पत्ता" तो कई बार सुनी होगी, फिर नया क्या होता। मुझे हरिहरण प्रिय हैं, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती है और इसी कारण मैं चाहता था कि बाकी मित्र भी उनकी आवाज़ से रूबरू हो लें। दक्षिण भारत से संबंध रखने के बावजूद उर्दू के शब्दों को वो जिस आसानी से गाते हैं और जितनी तन्मयता से वो हर लफ़्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान देते हैं, उतनी मेहनत तो हिंदी/उर्दू जानने वाला एक शख्स नहीं करता। मेरे हिसाब से हरिहरण की ग़ज़ल सुनी जानी चाहिए.. हाँ, आप इनकी ग़ज़लों की तुलना मेहदी हसन या गुलाम अली से तो नहीं हीं कर सकतें, वे सब तो इस कला के उस्ताद हैं, लेकिन यह कहाँ लिखा है कि उस्ताद के सामने शागिर्द को मौका हीं न मिले। मेरी ख्वाहिश बस यही मौका देने की थी... कितना सफल हुआ और कितना असफल, ये तो बाकी मित्र हीं बताएँगे। अवनींद्र जी और शन्नो जी, आप दोनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें शुभकामनाएँ दीं, हमारी तरफ़ से भी आप सभी स्वजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ.. मराठी में कहें तो "शुभेच्छा".. महाराष्ट्र में रहते-रहते यह एक शब्द तो सीख हीं गया हूँ :)
चलिए तो इन्हीं बातों के साथ अगली महफिल तक के लिए अलविदा कहते हैं। खुदा हाफ़िज़!
प्रस्तुति - विश्व दीपक
ग़ज़लों, नग्मों, कव्वालियों और गैर फ़िल्मी गीतों का एक ऐसा विशाल खजाना है जो फ़िल्मी गीतों की चमक दमक में कहीं दबा दबा सा ही रहता है. "महफ़िल-ए-ग़ज़ल" श्रृंखला एक कोशिश है इसी छुपे खजाने से कुछ मोती चुन कर आपकी नज़र करने की. हम हाज़िर होंगे हर बुधवार एक अनमोल रचना के साथ, और इस महफिल में अपने मुक्तलिफ़ अंदाज़ में आपके मुखातिब होंगे कवि गीतकार और शायर विश्व दीपक "तन्हा". साथ ही हिस्सा लीजिये एक अनोखे खेल में और आप भी बन सकते हैं -"शान-ए-महफिल". हम उम्मीद करते हैं कि "महफ़िल-ए-ग़ज़ल" का ये आयोजन आपको अवश्य भायेगा.




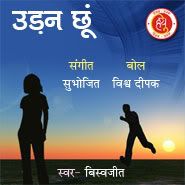


 संस्कार गीतों पर एक विशेष शृंखला
संस्कार गीतों पर एक विशेष शृंखला मन जाने - विवधताओं से भरी अल्बम
मन जाने - विवधताओं से भरी अल्बम








 लता मंगेशकर जब मिली आवाज़ के श्रोताओं से
लता मंगेशकर जब मिली आवाज़ के श्रोताओं से द रिटर्न ऑफ आलम आरा प्रोजेक्ट एक कोशिश है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म के गीत संगीत को फिर से रिवाईव करने की, सहयोग दें, और हमारी इस नेक कोशिश का हिस्सा बनें
द रिटर्न ऑफ आलम आरा प्रोजेक्ट एक कोशिश है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म के गीत संगीत को फिर से रिवाईव करने की, सहयोग दें, और हमारी इस नेक कोशिश का हिस्सा बनें 

 सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन यानी इंडस्ट्री के दाद्दु पर एक विशेष शृंखला जिसके माध्यम हम सलाम कर रहे हैं फिल्म संगीत जगत में, इस अदभुत कलाकार के सुर्रिले योगदान को
सुप्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन यानी इंडस्ट्री के दाद्दु पर एक विशेष शृंखला जिसके माध्यम हम सलाम कर रहे हैं फिल्म संगीत जगत में, इस अदभुत कलाकार के सुर्रिले योगदान को लोरियों की मधुरता स्त्री स्वर के माम्तत्व से मिलकर और भी दिव्य हो जाती है. पर फिल्मों में यदा कदा ऐसी परिस्थियों भी आई है जब पुरुष स्वरों ने लोरियों को अपनी सहजता प्रदान की है. पुरुष स्वरों की दस चुनी हुई लोरियाँ लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं ओल्ड इस गोल्ड में इन दिनों
लोरियों की मधुरता स्त्री स्वर के माम्तत्व से मिलकर और भी दिव्य हो जाती है. पर फिल्मों में यदा कदा ऐसी परिस्थियों भी आई है जब पुरुष स्वरों ने लोरियों को अपनी सहजता प्रदान की है. पुरुष स्वरों की दस चुनी हुई लोरियाँ लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं ओल्ड इस गोल्ड में इन दिनों 

 शक्ति के बिना धैर्य ऐसे ही है जैसे बिना बत्ती के मोम।
शक्ति के बिना धैर्य ऐसे ही है जैसे बिना बत्ती के मोम।



आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)
6 श्रोताओं का कहना है :
शब्द है बला वैसे तो इस शब्द के दो तरह से अर्थ निकलते हैं मगर यहाँ जो अर्थ है उसी पे शेर अर्ज़ है
वो जब चाहे छीन ले मुझको ही मुझसे
उनकी बला से फिर में भले तड़पता ही रहूँ (स्वरचित)
जल गया दिल मगर ऐसी जो बला निकले है
जैसे लू चलती मेरे मुँह से हवा निकले है।
(मीर तक़ी ’मीर’)
उनकी बला से जीउँ या मरूँ मैं ,
उनकी आदत रिवाज बन गई रे !
गायब वाला शब्द है ' बला ' ..इस पर एक शेर प्रस्तुत है :
बला की हसीन शाम थी
न जाने किसके नाम थी
लम्हा-लम्हा गुजर गयी
तन्हाई बची मेरे नाम थी.
( स्वरचित )
सुनते है की मिल जाती है हर चीज दुआ से
एक रोज़ तुम्हे मांग के देखेंगे खुदा से
आईने में वो अपनी अदा देख रहे है
मर जाये की मिट जाये कोई उनकी बला से
------------सोहेल राना
तमन्ना फिर मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ
यह मौसम ही बदल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ
ये दुनिया भर के झगड़े, घर के किस्से, काम की बातें
बला हर एक टल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ
-----------जावेद अख्तर
--------------------------------------------आशीष
येथे फिर से आई हूँ...सरबत पीकर :)
साथ में फिर से बला लाई हूँ...
रुतबा है जिनका ना आपे में वो हैं
सरे आम मुल्क में तबाही मची है
न है परवाह उनको उनकी बला से
इज्ज़त लुटी या किसी की बची है.
स्वरचित ही है...
आप क्या कहना चाहेंगे? (post your comment)